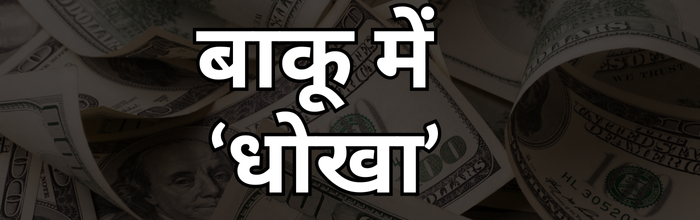प्लास्टिक संधि पर भारत की उलझन, एक ओर प्रदूषण तो दूसरी ओर रोज़गार खोने का संकट
प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में अंतर्राष्ट्रीय बैठक चल रही है। पेट्रोलियम समृद्ध देश प्लास्टिक उत्पादन को कम नहीं करना चाहते और कचरे के मैनेजमेंट पर ज़ोर दे रहे हैं। भारत अपने बड़े प्लास्टिक उत्पादन वर्कफोर्स को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन चाहता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है?
अज़रबैजान की राजधानी बाकू में जलवायु वार्ता (COP29) में कुछ खास निकल कर नहीं आया। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को घटाने और जलवायु संकट से लड़ने के लिए फाइनेंस के मुद्दे पर कोई उल्लेखनीय तरक्की नहीं हुई बल्कि वार्ता को पूरी तरह असफल माना जा रहा है। अब इसके तुरंत बाद, 175 देश वैश्विक प्लास्टिक संधि (जीपीटी) पर अंतिम दौर की वार्ता के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में जुट गये हैं। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी को लेकर बढ़ी चिंता के बीच भी हो रही है। जीवाश्म ईंधन विस्तार के लिए नए सिरे से प्रयास का संकेत दे सकता है।
इस संधि पर आम सहमति बनाना महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि प्लास्टिक पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, साथ ही उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर इसकी भारी निर्भरता के कारण जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। जबकि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना बुसान में एजेंडे में शीर्ष पर होगा, वार्ताकारों को ऐसी संधि के भूराजनीतिक निहितार्थों पर भी ध्यान देना होगा।
कोई आश्चर्य नहीं कि प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ़ अपील के बावजूद, जीवाश्म-ईंधन-समृद्ध देश प्लास्टिक में अपने आर्थिक हितों को संरक्षित करने के इच्छुक हैं। ये जीवाश्म-ईंधन-समृद्ध देश वर्तमान में प्लास्टिक उत्पादन पर अंकुश लगाने के उपायों को अपनाने का विरोध कर रहे हैं, और इसके बजाय केवल अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग पर केंद्रित समाधानों की वकालत कर रहे हैं।
ऐसी परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं पर बातचीत जटिल हो जाती है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत में एक बड़ा वर्ग प्लास्टिक उद्योग से जुड़ा है जो ज़्यादातर छोटे और मझौले उद्यम हैं। अब सवाल है ऐसे में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए बढ़ते वैश्विक दबाव के सामने भारत आर्थिक विकास और टिकाऊ प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे हासिल कर सकता है?
वैश्विक प्लास्टिक संधि की शुरुआत
पहले प्लास्टिक पॉलिमर का आविष्कार 1869 में हुआ था, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा कितना व्यापक है यह तथ्य इसके सौ साल बाद 1970 और 1980 के दशक में स्वीकार किया गया। प्रारंभ में, देशों की चिंता मुख्य रूप से समुद्र में जमा हो रहे प्लास्टिक तक ही सीमित थी। महज़ दस साल पहले, 2014 में, केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के पहले सत्र में, “समुद्री प्लास्टिक मलबे और माइक्रोप्लास्टिक” को मुख्य मुद्दों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भारत ने 2019 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया।
प्लास्टिक सस्ती, सिंथेटिक सामग्री है जो मुख्य रूप से पॉलिमर से बनी होती है, जिन्हें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से तैयार किया जाता है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के उत्पादन में वृद्धि का सीधा संबंध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि से है। इसके अलावा प्लास्टिक खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित करने, पानी और मिट्टी को दूषित करने और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर पारिस्थितिक प्रभाव भी खराब कर रहा है।
पृथ्वी पर प्लास्टिक के बढ़ते खतरे के बीच, दुनिया के देशों ने मार्च 2022 में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करने पर सहमति व्यक्त की – जिसे वैश्विक प्लास्टिक संधि (जीपीटी) के रूप में भी जाना जाता है – जिसका उद्देश्य “प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना” है। “उत्पादन, डिजाइन और निपटान सहित प्लास्टिक के पूर्ण जीवन चक्र को संबोधित करने वाले व्यापक दृष्टिकोण” पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतर सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का लक्ष्य 2024 के अंत तक वार्ता पूरी करने का है।
प्रारंभ में यह संधि पेरू और रवांडा द्वारा प्रस्तावित की गई और इसे भारत सहित 175 देशों का समर्थन प्राप्त है। आज तक, उरुग्वे, फ्रांस, केन्या और कनाडा में चार दौर की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्र आम सहमति की दिशा में काम कर रहे हैं। पांचवें और अंतिम दौर की चर्चा 25 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक दक्षिण कोरिया में होने वाली है।
प्लास्टिक से जुड़े कुछ तथ्य
| प्लास्टिक उत्पादन में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी खतरे 1950 में दुनिया भर में केवल 1.5 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता था और 2022 में यह आंकड़ा 400 करोड़ टन तक पहुंच गया। 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उस कुल उत्सर्जन का 15 प्रतिशत होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए अधिकतम सीमा है। आज हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है। यह आंकड़ा 2040 तक तीन गुना हो सकता है। समुद्री कचरे में 85% हिस्सा प्लास्टिक का है। लगभग 800 समुद्री और तटीय प्रजातियाँ प्लास्टिक निगलने या इसमें उलझने सहित विभिन्न तरीकों से खतरे में हैं। कुल प्लास्टिक कचरे में 60% से अधिक हिस्सा सिंगल यूज़ (एकल उपयोग) प्लास्टिक का है। |
संधि की बारीकियों पर खींचतान
इस संधि का दायरा बहुत बड़ा है, जो प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र पर केंद्रित है – कच्चे माल के निष्कर्षण से लेकर डिज़ाइन, रासायनिक उपयोग, कचरे के निपटान और रीसाइक्लिंग तक। मार्च 2022 में, जब यूएनईए में प्लास्टिक संधि के लिए प्रस्ताव अपनाया गया था, तो इसे “पेरिस समझौते के बाद से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण बहुपक्षीय समझौता” कहा गया। रवांडा और नॉर्वे के नेतृत्व में, 40 देशों को मिलाकर एक “हाई एम्बिशन गठबंधन” (एचएसी) का गठन किया गया, जो 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण के उन्मूलन की बात करता है। यह ब्लॉक एक ऐसे समझौते पर ज़ोर दे रहा है जो प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र (कच्चा माल निकालने से लेकर कचरे के निस्तारण तक) में हस्तक्षेप की गारंटी देता है।
पेरू और रवांडा द्वारा ओटावा सम्मेलन (INC-4) में ’40 x 40′ नाम का एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 2040 के अंत तक प्लास्टिक उत्पादन में 40% की कटौती करना है। कुल 27 देशों के समर्थन के साथ, ओटावा सम्मेलन संपन्न हुआ। एक घोषणा के साथ – ब्रिज टू बुसान – यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि “उत्पादन में कटौती” बुसान शिखर सम्मेलन के एजेंडे में बनी रहे।
हालाँकि, आगे संभावित बाधाएँ हो सकती हैं। सऊदी अरब, रूस, अमेरिका और ईरान जैसे बड़े तेल, पेट्रोकेमिकल लॉबी और पेट्रोस्टेट सामग्री के निष्कर्षण (खनन और ड्रिलिंग आदि) और प्लास्टिक के उत्पादन (जिसे प्लास्टिक चक्र के “अपस्ट्रीम” चरण के रूप में जाना जाता है) को कम नहीं करना चाहते हैं। वे केवल “डाउनस्ट्रीम” चरण को संबोधित करने की वकालत कर रहे हैं, जिसमें रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। वास्तव में, सऊदी अरब, ईरान, रूस, चीन और क्यूबा जैसे देशों ने “प्लास्टिक सस्टेनेबिलिटी के लिए वैश्विक गठबंधन” गठबंधन बनाया है ताकि यह मांग की जा सके कि संधि को उत्पादन पर नहीं बल्कि कचरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जीवाश्म ईंधन को खपाने के खातिर
पिछले साल यूएई जलवायु सम्मेलन (कॉप-28) में ली गई प्रतिज्ञा के तहत, दुनिया को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा और कम कार्बन पथ पर “संक्रमण” (ट्रांजिशन अवे) करना होगा। स्वाभाविक रूप से, तेल और गैस-समृद्ध देश अपने जीवाश्म ईंधन के लिए अन्य रास्ते तलाश रहे हैं। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के प्रोग्राम मैनेजर सिद्धार्थ घनश्याम सिंह के अनुसार, प्लास्टिक उद्योग इन देशों के लिए जीवाश्म ईंधन खपाने का ज़रिया बनेगा।
सिंह के मुताबिक, “जीवाश्म ईंधन से समृद्ध देश और मेगा तेल और गैस कंपनियां जीवाश्म ईंधन के उपयोग या निष्कर्षण को कम नहीं करेंगी। उनका कहना है कि अगर आप बिजली उत्पादन में कोयला, गैस और तेल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे तो हम इसका इस्तेमाल करने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे।”
आश्चर्य नहीं कि प्लास्टिक लॉबीकर्ताओं और पैरोकारों (जो जीवाश्म ईंधन और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के प्रतिनिधि हैं) की संख्या अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं बढ़ रही है और वह संधि के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ओटावा, कनाडा में पिछली संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि बैठक में, केन्या के नैरोबी में आयोजित पिछले सम्मेलन में उनकी उपस्थिति की तुलना में ऐसे लॉबीकर्ताओं की संख्या एक तिहाई बढ़ गई।
यह पेरू, रवांडा और नॉर्वे जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है, जो नहीं चाहते कि प्लास्टिक का उत्पादन बढ़े। वे बुसान (आईएनसी-5) में कड़ी सौदेबाजी करने की योजना बना रहे हैं। सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायर्नमेंटल लॉ (सीआईईएल) की पेट्रोकेमिकल्स अभियान प्रबंधक डेल्फ़िन लेवी अल्वारेस के अनुसार, “बुसान में सहमत संधि में जो लिखा जायेगा वह तय करेगा कि विश्व स्तर पर प्लास्टिक नीति की गवर्नेंस कैसी होगी”
अल्वारेस ने कहा, “अगर बातचीत करने वाले देश ऊंचे इरादे या महत्वाकांक्षा रखें तो तो हम इन वजहों को हल कर सकते हैं कि कितना प्लास्टिक पैदा किया जा रहा है, उसे बनाने में कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है और हम उसे कचरे के रूप में कैसे प्रबंधित करते हैं। बड़े पॉलिमर उत्पादकों, रसायन निर्माताओं और अन्य व्यावसायिक हितों से जुड़े लोगों का बड़ा पैसा दांव पर है, और उनके पैरवीकार संभवतः एक मजबूत ताकत के रूप में सामने आएंगे।
सीआईईएल द्वारा अन्य स्वदेशी और नागरिक समाज समूहों के सहयोग से किए गए एक विश्लेषण में पाया गया कि कुल 196 जीवाश्म ईंधन और रासायनिक उद्योग के पैरवीकारों ने आईएनसी-4 में पंजीकरण कराया था, जो संख्या आईएनसी-3 के मुकाबले 37% की वृद्धि है। INC-4 में, जीवाश्म ईंधन और रासायनिक उद्योगों ने जितने प्रतिनिधि भेजे उनकी संख्या दुनिया के 87 सबसे छोटे प्रतिभागी देशों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडलों से अधिक है।
अल्वारेस कहती हैं, “लॉबीकर्ता तमाम देशों के प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य के रूप में आ रहे हैं और इस कारण उनकी पहुंच सदस्य देशों के विशेषाधिकार प्राप्त सत्रों तक हो जाती है, जहां संवेदनशील चर्चाएं बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। इससे पता चलता है कि उद्योग में पैरवी करने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।”
भारत की उलझन
आईएनसी में, भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि को विशेष रूप से केवल प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करना चाहिए” और “प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन के संबंध में कोई बाध्यकारी लक्ष्य/सीमा नहीं होनी चाहिए।” अपने दस्तावेज़ के ‘प्रस्तावित सिद्धांत’ खंड में, भारत ने मांग की है कि संधि “सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी [सीबीडीआर] के सिद्धांत के साथ-साथ राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए…”
भारत की अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक का बढ़ता महत्व अंतरराष्ट्रीय मंच पर जीपीटी पर उसके रुख को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्लास्टिक उद्योग में लगभग 130,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत और लगे हुए हैं, जिन्होंने लगभग 1.65 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। प्लास्टिक उद्योग भारत में 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। प्लास्टिक उत्पादन में किसी भी कटौती के भारत के विरोध के पीछे यह प्राथमिक कारणों में से एक है।
एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कार्बनकॉपी को बताया, “भारत ऐसा रुख क्यों अपनायेगा जो उसके अपने देश में लोगों को बेरोजगार कर दे? अमीर देशों ने दशकों तक प्लास्टिक का उत्पादन और उपयोग किया और पृथ्वी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित किया। अब वह इसका दोष विकासशील देशों पर डाल रहे हैं। सच तो यह है कि प्लास्टिक लाखों लोगों को नौकरियाँ प्रदान करता है। यहां तक कि कचरा भी कई उद्यमियों के लिए अवसर पैदा करता है, ”।
2014 में, भारत में प्लास्टिक मशीनरी का कुल उत्पादन मूल्य ₹21.5 बिलियन था। 2022 में, यह ₹38.5 बिलियन तक पहुंच गया – एक दशक से भी कम समय में लगभग 80% की वृद्धि। वित्त वर्ष 2022-23 में प्लास्टिक से संबंधित सामग्री का संचयी निर्यात 11.96 बिलियन डॉलर था।
देश के भीतर प्लास्टिक की चुनौती
पिछले 30 वर्षों में, भारत में प्लास्टिक की खपत 20 गुना से अधिक बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति खपत अब 15 किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालाँकि यह अमेरिका की प्रति व्यक्ति खपत (108 किग्रा) से काफी कम और वैश्विक औसत (30 किग्रा) का आधा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) और प्रैक्सिस ग्लोबल एलायंस के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में प्लास्टिक की खपत प्रति वर्ष लगभग 10% बढ़ रही है, लेकिन इससे उत्पन्न कचरा सालाना 20% बढ़ रहा है। |
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक समस्या नहीं है, केवल प्लास्टिक कचरा ही समस्या है। उनका कहना है कि प्रदूषण “प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के कारण होता है” और “प्लास्टिक का उपयोग समाप्त करना कोई आसान समाधान नहीं है।”
भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के गैर-लाभकारी एकीकृत संघ के अध्यक्ष राजीव चावला कहते हैं, “कोई भी प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। क्या आप प्लास्टिक का उपयोग किए बिना कार, मिक्सर या वॉशिंग मशीन बना सकते हैं? प्लास्टिक जिसका उपयोग लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं और अन्य बहुमूल्य पर्यावरणीय संसाधनों को बचाने के लिए किया जाता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समय की मांग है कि अल्पकालिक उपयोग वाले प्लास्टिक का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाए और हम निश्चित रूप से इसके लिए कदम उठा रहे हैं।” इस मुद्दे पर भारत के रुख को बेहतर ढंग से समझने के लिए कार्बनकॉपी ने MoEFCC से संपर्क किया। प्रतिक्रिया प्राप्त होते ही इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा।
इस सोच के अनुरूप, भारत घरेलू मोर्चे पर प्लास्टिक की रिसायक्लिंग करने, इसे “अपशिष्ट-से-ऊर्जा” संयंत्रों में उपयोग करने और इसे भस्मक में भेजने का प्रयास कर रहा है। कचरे को कम करने के लिए, सरकार ने अगस्त 2021 में “चिह्नित एकल उपयोग (सिंगल यूज़) प्लास्टिक वस्तुओं” पर प्रतिबंध की घोषणा की। यह आदेश जुलाई 2022 में लागू हुआ, जिसके तहत सरकार ने “पहचानित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं” पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनकी उपयोगिता कम है और कूड़ा अधिक फैलता है।” मिसाल के तौर पर प्लास्टिक स्टिक्स, ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें और सिगरेट के पैकेट, अन्य। हालाँकि, ज़मीनी स्तर पर यह आदेश शायद ही कभी लागू किया जाता है और काफी हद तक अप्रभावी साबित हुआ है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली की वरिष्ठ फैकल्टी पारमिता डे कहती हैं, “प्लास्टिक का संग्रह तभी संभव है जब यह साफ हो और स्रोत पर अलग किया गया हो। अन्यथा, उपभोक्ता के बाद प्लास्टिक का संग्रह बेहद चुनौतीपूर्ण है। डे के अनुसार, प्लास्टिक पैकेजिंग कुछ वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई अन्य उत्पादों में इससे बचा जा सकता है।
पारमिता के मुताबिक, “जब तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उत्पादन पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, यह हमारे पर्यावरण से बाहर नहीं निकल पाएगा। बहुत सारे एमएसएमई एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन में शामिल हैं। इसे चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत है और उनके लिए विकल्प प्रस्तावित किए जाने चाहिए।”
एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के साथ, भारत ने पैकेजिंग उद्योग में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) व्यवस्था भी शुरू की है। यह ईपीआर व्यवस्था, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कार्य करती है, “रीसाइक्लिंग, पुन: उपयोग या जीवन के अंत के निपटान के माध्यम से अपने प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की रिसायकिलिंग को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों (पीआईबीओ) की जिम्मेदारी बताती है।”
ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत, पीआईबीओ और अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं (जिन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रक्रिया या पीडब्ल्यूपी के रूप में जाना जाता है) को केंद्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईपीआर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। जबकि नियम विशिष्ट लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं, ईपीआर व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में कई कमजोरियां हैं। यह मुख्य रूप से पैकेजिंग प्लास्टिक कचरे को संबोधित करता है, जिससे सैनिटरी नैपकिन और चप्पल जैसी कई वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
“वेस्टेड” पुस्तक के लेखक और टेक्नोपैक एडवाइजर्स के सीनियर पार्टनर अंकुर बिसेन कहते हैं कि वर्तमान में नीति निर्माता “एक बहुत ही जटिल समस्या के लिए एक बहुत ही सरल ढांचे” का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पैट (पीईटी) बोतलों को ज्यादातर पुनर्चक्रित किया जाता है और मूल्य श्रृंखला में वापस लाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिंगल लेयर प्लास्टिक (एसएलपी) और मल्टी लेयर प्लास्टिक (एमएलपी) को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता हो।
बिसेन ने कार्बनकॉपी को बताया, “एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर, हम केवल मुद्दे के उस हिस्से को संबोधित कर रहे हैं जो हाशिए पर रहने वाले, एकल इकाई खुदरा विक्रेताओं या दुकानदारों को प्रभावित करता है। हमने एमएलपी और एसएलपी के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है, जिनका कोई पुनर्चक्रण मूल्य नहीं है और जिन्हें केवल जलाया जा सकता है। वे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ उन्हें नियंत्रित नहीं करती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि एफएमसीजी [तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं] अपने उत्पादों जैसे चिप्स, केचप आदि के लिए प्राथमिक पैकेजिंग समाधान के रूप में छोटे प्लास्टिक बैग में एमएलपी और एसएलपी का उपयोग कर रहे हैं जो हर जगह फैलते हैं। सभी एफएमसीजी की वृद्धि एमएलपी और एसएलपी पर आधारित है और यह लगातार अस्थिर होती जा रही है।’
अभिषेक गर्ग, जो एक ईपीआर सलाहकार हैं, बताते हैं कि भारत की ईपीआर व्यवस्था कंपनियों को अपने उत्पादों के पैकेजिंग कचरे को इकट्ठा करने और स्थायी रूप से संसाधित करने का आदेश देती है। कंपनियां अब सरकार द्वारा अधिकृत रिसाइक्लर्स से ईपीआर क्रेडिट खरीद सकती हैं, जो अनिवार्य रूप से रिसाइक्लर्स को प्रोत्साहित करती हैं। यूरोपीय संघ में व्यापक रूप से अपनाई गई यह क्रेडिट-आधारित प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बाध्य कंपनियाँ या तो अनुपालन करें या दंड का सामना करें।
प्रारंभिक अधिसूचना के बाद से ईपीआर दिशानिर्देशों में आधा दर्जन से अधिक संशोधनों के बावजूद, महत्वपूर्ण खामियां बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, 6 लाख से अधिक नकली प्रदूषण-व्यापार प्रमाणपत्रों का पता चलना इस मुद्दे को उजागर करता है।
गर्ग कहते हैं, “यूरोप में, इस प्रणाली को सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश के साथ-साथ अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और रीसाइक्लिंग के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित किया जाता है। हालाँकि, भारत में, संग्रहण, स्रोत पृथक्करण और उपभोक्ता के बाद के कचरे के पुनर्चक्रण के लिए बुनियादी ढांचे की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। इसके अतिरिक्त, पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रोत्साहन देने से धोखाधड़ी की प्रथाओं को बढ़ावा मिला है, कुछ पुनर्चक्रणकर्ता गलत तरीके से पंजीकरण कर रहे हैं और नकली ईपीआर क्रेडिट तैयार कर रहे हैं।”
दुनिया भर में ईपीआर नीतियां ‘प्रदूषक भुगतान’ के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। उनका मूल लक्ष्य सामग्रियों के संग्रह, पुनर्चक्रण और परिपत्रता का समर्थन करना है। सीएसई के सिद्धार्थ घनश्याम सिंह का कहना है कि भारत में ईपीआर का कार्यान्वयन “बाज़ार संचालित” है और पूरी तरह से ईपीआर प्रमाणपत्रों के व्यापार पर आधारित है।
सिंह कहते हैं, “मुट्ठी भर पीडब्ल्यूपी ने जानबूझकर (7 लाख से अधिक) फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करके और पीआईबीओ के साथ व्यापार करके ईपीआर दिशानिर्देशों की अवहेलना की। परिणामस्वरूप, ईपीआर प्रमाणपत्रों की आपूर्ति बढ़ गई, जिससे उनकी कीमतें गिर गईं। इसके अलावा, विनियामक कार्रवाई केवल पीडब्लूपी पर की गई थी, न कि पीआईबीओ पर, जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र हासिल किए थे। प्रदूषकों को ‘मुक्त’ छोड़ देने का यह दृष्टिकोण उस मूल सिद्धांत को कमजोर करता है जिस पर ईपीआर नीतियां विश्व स्तर पर आधारित हैं।”
उत्पादन में कमी ज़रूरी
जो पर्यवेक्षक प्लास्टिक संधि वार्ता पर पर नज़र रख रहे हैं, उनका कहना है कि समस्या को अपस्ट्रीम चरण (उत्पादन वाला हिस्सा) को संबोधित किए बिना हल नहीं किया जा सकता है। भारत निश्चित ही आर्थिक चुनौतियों और मजबूरियों से घिरा है लेकिन फिर भी पेट्रो-समृद्ध राज्यों के साथ भारत का तालमेल उसे पर्यावरणीय जिम्मेदारी में खलनायक देशों के साथ खड़ा करता है।
केवल प्लास्टिक कटरे का प्रबंधन, भले ही वह बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया हो, संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सीआईईएल की अल्वारेस का कहना है कि उत्पादन सीमित करने के बारे में चर्चा से बचने में उत्पादकों की वित्तीय हिस्सेदारी है, लेकिन दुनिया अब प्लास्टिक उत्पादन जारी नहीं रख सकती है।
वह कहती हैं, “प्लास्टिक संकट को जड़ से खत्म करने के लिए उत्पादन कम करना न केवल व्यावहारिक रूप से संभव है, बल्कि बहुत आवश्यक भी है। 2022 में यूएनईए 5.2 में वार्ताकारों को दिए गए जनादेश में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था। प्लास्टिक प्रदूषण तब शुरू नहीं होता जब प्लास्टिक कचरा बन जाता है या पर्यावरण में समाप्त हो जाता है। यह तब शुरू होता है जब तेल, गैस और कोयले को धरती से निकालकर प्लास्टिक में बदला जाता है।”
अल्वारेस के मुताबिक, “कोई भी मांग-संचालित नीति उत्पादित प्लास्टिक की कुल मात्रा और इसके साथ होने वाले प्रदूषण को कम करने में सफल नहीं रही है, क्योंकि उद्योग को बस नए बाजार और उत्पाद मिलते हैं। प्लास्टिक उत्पादन को कम किए बिना हम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान नहीं कर पाएंगे।”
जलवायु कार्यकर्ता और फॉसिल फ्यूल नॉन-प्रोलिफिरेशन ट्रीटी इनीशिएटिव के ग्लोबल इंगेज़मेंट निदेशक हरजीत सिंह का कहना है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए, किसी को जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक और जीवाश्म ईंधन उद्योग के बढ़ते प्रभाव के बीच आंतरिक संबंध को पहचानना होगा।
सिंह ने कार्बनकॉपी को बताया, “नई वैश्विक प्लास्टिक संधि को प्लास्टिक प्रदूषण के मूल कारण: जीवाश्म ईंधन को संबोधित करके पिछले जलवायु समझौतों की भूलों को दूर करना चाहिए। यह संधि उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती है जो हम सभी जानते हैं – कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का मतलब जीवाश्म ईंधन-आधारित प्लास्टिक को स्रोत पर रोकना है। बहुत लंबे समय से, कॉर्पोरेट हितों ने हमारे ग्रह और लोगों की भलाई के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दी है। हमें प्लास्टिक उत्पादन को रोकने और भविष्य की पीढ़ियों को जीवाश्म-ईंधन-संचालित प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के जटिल संकट से बचाने के लिए बिना झुके साहसिक, कार्रवाई की आवश्यकता है।
हालाँकि, सवाल यह है कि भारत जैसा विशाल देश अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। बिसेन इसके लिए “न्यायसंगत परिवर्तन के रोडमैप” की वकालत करते हैं।
वह कहते हैं, “पुनर्चक्रण को एक स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए और हमें निश्चित रूप से इसके उत्पादन (को कम करने ) पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए, हमें एक उचित परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की आवश्यकता है, ताकि कंपनियां और व्यवसाय धीरे-धीरे अपने सिस्टम से प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने का लक्ष्य बढ़ा सकें। नीति निर्माताओं को बड़े और छोटे व्यवसायों के लिए सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित करना चाहिए – उदाहरण के लिए मोबिल ऑयल के लिए प्लास्टिक कंटेनरों के बजाय टिन के डिब्बे की बहाली हो, ताकि मूल्य श्रृंखला में कोई व्यवधान न हो या आजीविका का नुकसान न हो।’
भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए यह बड़ा जोखिम है जो प्लास्टिक प्रदूषण से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं और फिर भी इसके आर्थिक लाभों पर निर्भर हैं। कॉप29 और बुसान शिखर सम्मेलन दोनों के परिणामों को आदर्श रूप से प्लास्टिक कचरे और उत्पादन के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को आकार देने में मदद करनी चाहिए। यह अंततः वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने का मार्ग निर्धारित करेगा।
बाकू में खींचतान की कहानी: विकसित देशों ने कैसे क्लाइमेट फाइनेंस के आंकड़े को $300 बिलियन तक सीमित रखा
एक बार फिर जलवायु वित्त समझौते में सत्ता, संघर्ष और लंबे समय से चली आ रही असमानताओं का पर्दाफाश हुआ।
विकसित देश बाकू में कॉप29 में वही रहस्यमय भाव चेहरों पर लिए आये, जो हर जलवायु वार्ता में उनका लिबास होता है। एक पहेली वाला भाव और अंतिम क्षणों तक पत्ते न खोलने की फितरत। विकासशील देशों के लिए, यह अक्सर बड़ी परेशानी का संकेत होता है: परदे के पीछे बन्द कमरों में होने वाले सौदों की प्रस्तावना जो कमजोर समुदायों की तत्काल और अस्तित्व संबंधी जरूरतों को दरकिनार करते हुए अमीर देशों के लिए जीत का रास्ता सुनिश्चित करती है।
इस वर्ष, $100 बिलियन के वर्तमान जलवायु वित्त लक्ष्य को तीन गुना बढ़ाकर $300 बिलियन कर दिया गया – यह एक सुर्खियाँ बटोरने वाला आंकड़ा था। लेकिन बारीकी से देखें तो इस तीन गुने में कुछ भी उत्साहित करने वाला नही बल्कि यह कई चेतावनियों से भरा हुआ था। पैकेज में सरकारी और निजी फाइनेंस का मिश्रण था। अनुदान और मदद के रूप में जो दिया जाना था वह $1.3 ट्रिलियन की उस राशि से बहुत दूर था, जिसकी जी77+ चीन समूह ने पहले मांग की थी। विकसित देशों ने विकासशील देशों से योगदान का आह्वान किया जिससे निराशा और बढ़ गई।
क्लाइमेट विशेषज्ञ और आईआईएम कोलकाता की प्रोफेसर रूना सरकार ने कहा, “2024 में दुनिया भर में चुनाव होने और कोविड के बाद से राष्ट्रीय बजट में गिरावट के बाद, 2025 में पहले ही कटौती तय थी। इसके आलोक में, 2035 से प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर का मामूली वादा बहुत हैरान करने वाला नहीं है”।
जैसे-जैसे सम्मेलन समाप्त हुआ, यह प्रश्न पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया: क्या कॉप29 एक जीत थी या दुनिया ने एक और अवसर को दिया? उत्तर, हमेशा की तरह, दृष्टिकोणों के पेचीदा मिश्रण और जलवायु अन्याय की अनसुलझी वास्तविकता में निहित है।
एक धीमी शुरुआत
“वे [विकसित देश] अपने पत्ते मेज पर नहीं रख रहे हैं।” विकासशील देशों के प्रतिनिधिमंडल और विशेषज्ञ कॉप29 के दो चरणों में यही बात दोहराते रहे। यह सम्मेलन तो “फाइनेंस केंद्रित” होना था। और फिर भी, 11 नवंबर को शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही, सभी संकेत थे कि कुछ बड़ा होने नहीं जा रहा। इस सम्मेलन में कोई बड़ा नेता नहीं था, और इसलिए कोई बड़ी आवाज़ भी नहीं थी – जिसने अतीत में बातचीत के गतिरोध को दूर करने में मदद की हो। पहले सप्ताह में ही अर्जेंटीना के वॉक आउट से अनिश्चितता और बढ़ गई। राजनीतिक इच्छाशक्ति की यह कमी जल्द ही नागरिक समाज समूहों के लिए सबसे चिंताजनक मुद्दा बनी।
यह सब और निश्चित रूप से, कॉप29 के जलवायु वित्त पाठ में एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) को लेकर ठंडा रुख जो कि सम्मेलन की शुरुआत में वार्ता का प्रमुख बिंदु था। एनसीक्यूजी ने अब तक के 100 अरब डॉलर के जलवायु वित्त लक्ष्य की जगह पेश किया गया मैकेनिज्म है जो विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को भुगतान करने के लिए निर्धारित किया गया था।
लेकिन वार्ता के लगातार दौरों के बाद संधि का जो टेक्स्ट आ रहा था उसमें एक प्रश्न चिन्ह था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि इस पैसे का भुगतान कैसे किया जाना था। सार्वजनिक वित्त के माध्यम से, जिसमें अनुदान शामिल होगा? या निजी वित्त के माध्यम से? क्या वित्त के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण होगा? वास्तव में पैसा कब और कहां से आना शुरू होता है? इन सवालों के जवाब बाकू ओलंपिक स्टेडियम के लंबे गलियारों में बस फुसफुसाहट और अटकलें ही लगाई गईं, लेकिन शिखर सम्मेलन के आखिरी कुछ दिनों तक कभी भी कोई ठोस तथ्य नहीं बताया गया। पहला रहस्य जिसे सुलझाने की जरूरत थी वह यह था कि इस “फाइनेंस सीओपी” में एनसीक्यूजी नंबर क्यों नहीं बताया जा रहा था। किसी संख्या की गणना करने के लिए देशों के पास पूरा एक वर्ष होता था। तो किसने अपना होमवर्क नहीं किया था?
पहले सप्ताह में ही हमें पता चला कि जी77 + चीन ने वास्तव में सार्वजनिक वित्त में प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन की एनसीक्यूजी संख्या का प्रस्ताव रखा था। पहले चर्चा की जा रही थी कि ट्रिलियन डॉलर की जलवायु वित्त आवश्यकता की घोषणा पहली बार भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत 2023 में नई दिल्ली घोषणा में की गई थी। भारत ने इस साल मार्च में जलवायु वित्त में 1 ट्रिलियन डॉलर का प्रस्ताव भी संयुक्त राष्ट्र को सौंपा था। यह महत्वाकांक्षी था, विशेष रूप से यह देखते हुए कि विकसित देशों ने 2022 में ही पिछले 100 अरब डॉलर के लक्ष्य का भुगतान बड़ी मुश्किल से किया जबकि इसका वादा 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में किया जा चुका था।
1.3 ट्रिलियन डॉलर की संख्या विश्लेषण पर आधारित थी जिसमें विकासशील दुनिया की जरूरतों की गहन गणना की गई थी।इसके बावजूद बारा बार आ रहे संधि के टेक्स्ट में इसे जगह नहीं मिली। यह विकसित देशों द्वारा दूसरे पक्ष को थका देने की एक सोची-समझी रणनीति थी जब तक कि उनकी संख्या को अंततः स्वीकार नहीं कर लिया गया। बाद में यही हुआ भी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विशेष राष्ट्रपति दूत, जॉन केरी ने कॉप28 में घोषणा की थी कि अमेरिका के पास जलवायु वित्त के लिए कोई पैसा नहीं है। वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर देश होने के बावजूद अमेरिका ने पिछले साल लॉस एंड डैमेज फंड में मामूली 17 अरब डॉलर देने का वादा किया था। इसके बजाय, केरी ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के गठबंधन, ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो (जीएफएएनजेड) जैसे समूहों से जलवायु वित्त पाया जा सकता है। विकसित देशों ने जलवायु वित्त के एक हिस्से के रूप में कार्बन मार्केट्स को शामिल करने पर भी जोर दिया, जिससे कॉप29 में विकासशील देशों से बड़ा झटका लगा। पावर शिफ्ट अफ्रीका के संस्थापक और निदेशक मोहम्मद एडो ने कार्बन मार्केट्स को “भेड़ के भेष में ख़तरनाक भेड़िया” कहा जिसका मकसद सिर्फ ध्यान बंटाना है।
आखिरी काउंटडाउन
पहले सप्ताह में बार संधि का टेक्स्ट रिव्यू किया गया फिर दूसरे हफ्ते गुरुवार तक उपस्थित लोगों को पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जिन सदस्यों से कार्बनकॉपी ने बात की, वे निश्चित ही आशावादी थे, लेकिन विकसित देशों की एनसीक्यूजी संख्या क्या होगी, इसकी अनिश्चितता एक समस्या ज़रूर थी। विकासशील देशों का आरोप था किजलवायु वित्त बिल का भुगतान करने से बचने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को जारी पुनरावृत्ति में स्पष्ट था कि विकासशील देशों को निजी वित्त की ओर प्रोत्साहित करने और निवेश के लिए उपजाऊ जमीन बनाने वाली नीतियां लाने के लिए कहा गया था — यह अधिक निजी वित्त के लिए रास्ता बनाने का एक और प्रयास है। लेकिन संख्या पर सवाल बना रहा।
सम्मेलन में मौजूद पर्यवेक्षक हम जैसे लेखकों को व्यवहारिक होने की सलाह दे रहे थे। दिल्ली स्थित काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के सीनियर फेलो वैभव चतुर्वेदी ने कहा, “कम लागत, ब्याज मुक्त अनुदान के रूप में 1 ट्रिलियन डॉलर आने की उम्मीद कैसे की जाए। बातचीत के लिए यह ठीक है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम ऐसा होने की उम्मीद नहीं करते हैं
उनके मुताबिक, “यूरोपीय संघ [विकसित देशों की ओर से] आखिर में $300 बिलियन डॉलर देने की बात कह सकता था। विकासशील देश स्पष्ट रूप से $1 ट्रिलियन मांग रहे हैं। बीच में कहीं आप $500-600 मिलियन डॉलर मांग सकते हैं और यह आंकड़ा [सीओपी] अध्यक्ष और बाकी सभी को प्रोत्साहित करता है। वे कह सकते हैं ‘$500 बिलियन, जो कि $100 बिलियन की पिछली रकम की तुलना में 5 गुना है। यह उतना अच्छा नहीं है जितना विकासशील दुनिया मांग रही है अभी भी यह एक कामयाबी कही जा सकती है।”
एलएमडीसी और एडीजी के साथ जी77+ चीन के समूह ने देखा कि क्या होने वाला है और तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उन सभी ने कहा कि वे 600 अरब डॉलर के सार्वजनिक वित्त के आंकड़े को स्वीकार करेंगे और बाद में बड़े दावे के लिए काम करेंगे।
300 की मांग
शुक्रवार की रात इस खबर के साथ समाप्त हुई कि समापन सत्र शनिवार को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा – कॉप29 के आधिकारिक तौर पर समाप्त होने के एक दिन बाद। वह समय आया और चला गया लेकिन संधि में आखिरकार क्या लिखा जायेगा इस पर अनिश्चितता बनी रही। क्या विकासशील देश 250 अरब डॉलर को अस्वीकार कर देंगे? क्या वे और राशि की मांग करेंगे या वॉकआउट? “एक बुरे समझौते से अच्छा है कि कोई समझौता न हो” यह गूंज पूरे आयोजन स्थल पर सुनाई दे रही थी। विकासशील देशों के वार्ताकारों द्वारा 300 बिलियन डॉलर की मांग करने और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख रखने की कोशिश करने की सुगबुगाहट — जो विकसित देशों पर वित्तीय संसाधन प्रदान करने का दायित्व डालता है – का दौर शुरू हो गया।
बात आखिरी पल तक खिंच गई। आखिरकार संधि का टेक्स्ट लिखा जाना था और लोगों को वापस घर भी जाना था। आधी रात से ठीक पहले ही लिखित में बात साफ हुई। विकासशील देशों को 300 अरब डॉलर का वादा किया गया, लेकिन इसके लिए जुटाए गए वित्त के रूप में – सार्वजनिक, निजी और अन्य स्रोतों के माध्यम शामिल थे।
फिर खोया मौका
आलोचना के बावजूद, परिणाम पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आईं। अच्छी खबर? एक समझौता हुआ. बहुपक्षवाद शायद अभी भी बचा हुआ है। बुरी ख़बरें? विकासशील देशों में बदलावों का समर्थन करने के लिए आवंटित अपर्याप्त धनराशि के साथ, महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) की उम्मीदें कम बनी हुई हैं। विकसित देशों की वहां आगे बढ़ने में अनिच्छा बनी हुई है जहां यह मायने रखता है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की प्रोग्राम ऑफिसर, जलवायु परिवर्तन, सेहर रहेजा ने कहा, “महत्वाकांक्षी एनडीसी के लिए विकसित देशों का आह्वान इस सम्मेलन में लगातार सुना गया था, लेकिन एनडीसी में उच्च महत्वाकांक्षा को संभव बनाने के लिए साधन वास्तव में ज़रूरतों से मेल नहीं खाते हैं। वित्त कितना होगा इस बहस के अलावा, शमन, अनुकूलन, हानि और क्षति के लिए उप-लक्ष्यों की कमी; 10 वर्षों की टाइम लाइन (जो “2035 तक” है ) बहुत लंबी है और अनुदान समकक्ष वित्त पर जोर न दिये जाने से स्थिति और खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से चूक गया अवसर है।”
सच्चाई से दूर एक मरीचिका
सम्मेलन के समापन सत्र में, भारत ने दस्तावेज़ के अनुमोदन से ठीक पहले एक कड़ा हस्तक्षेप करते हुए, इस बात पर अपना गहरा असंतोष व्यक्त किया जिस तरीके संधि का टेक्स्ट स्वीकार करवाया गया । भारत की वार्ताकार चांदनी रैना ने प्रेसीडेंसी पर प्रक्रिया को “चरणबद्ध तरीके से प्रबंधित” करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि मेजबान ने विभिन्न घटनाओं पर समावेशी भावना का पालन नहीं किया है, साथ ही टेक्स्ट को अपनाने पर किसी भी निर्णय से पहले भारत को अपना बयान साझा नहीं करने दिया जैसा कि अनुरोध किया गया था।
चांदनी रैना ने कहा, “भारत लक्ष्य के प्रस्ताव को उसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है। जो राशि जुटाने का प्रस्ताव है वह बेहद कम है। यह एक मामूली रकम है. यह ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे देश के अस्तित्व के लिए आवश्यक अनुकूल जलवायु कार्रवाई में कोई मदद करेगा। यह दस्तावेज़ एक मरीचिका से अधिक कुछ नहीं है। हम इस दस्तावेज़ को अपनाने का विरोध करते हैं।”
कॉप29 के मुख्य वार्ताकार याल्चिन रफ़ीयेव ने जलवायु कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने के बारे में सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान पूरी तरह से “जलवायु कार्रवाई पर सहमति और महत्वपूर्ण निर्णयों को अपनाने” के प्रयासों पर था।
एक स्थानीय ने कार्बनकॉपी को बताया कि जिस दिन कॉप29 समाप्त हुआ, बाकू में सभी ने जश्न मनाया क्योंकि वे अब फिर से अपना जीवन जी सकते थे। सड़क और मेट्रो पर भीड़ से बचने के लिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कार्यालयों को घर से ही या दूर स्थान से संचालित करने का आदेश दिया गया था।
अब अगले साल ब्राज़ील में कॉप30 को पहले से ही “एनडीसी कॉप” कहा जा रहा है, जहाँ जीएसटी यानी आकलन का दूसरा दौर भी शुरू होगा।
बड़े पैमाने पर रोपण नहीं वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षण है मैंग्रोव को बचाने का उपाय
अनियंत्रित शहरीकरण और फंडिंग की चुनौतियों के बीच, स्थान-विशिष्ट पर वैज्ञानिक उपायों से मौजूदा मैंग्रोव संरक्षण करने से बड़े पैमाने पर रोपण की तुलना में बेहतर परिणाम मिले हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में चक्रवात और तूफान अधिक विनाशकारी होते जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में चक्रवात दाना ने भारत के पूर्वी तट पर तबाही मचाई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में व्यापक क्षति हुई। दुनिया भर में यही चिंताजनक प्रवृत्ति बनी हुई है। मिल्टन और हेलेन जैसे तूफान अमेरिका और एशिया में कहर बरपा रहे हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर गर्म होते जा रहे हैं, ऐसे तूफान बार-बार आ रहे हैं और तीव्र होते जा रहे हैं। ब्रिटेन स्थित क्रिश्चियन एड की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2023 में दुनिया में जिन जलवायु आपदाओं ने सबसे अधिक आर्थिक क्षति पहुंचाई थी उनमें 85% बाढ़ और उष्णकटिबंधीय तूफान थे।
इस दृष्टि से मैंग्रोव बढ़ते समुद्रों, चक्रवातों और तटीय कटाव के खिलाफ महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में काम कर सकते हैं। फिर भी, शहरीकरण और जलवायु पर दबाव के कारण ये इकोसिस्टम तेजी से कम हो रहे हैं। हालांकि भारत की मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल इनकम्स (मिष्टी) के तहत 540 वर्ग किमी तटरेखा पर फिर से वनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सबसे प्रभावी समाधान नहीं है।
तटीय सुरक्षा का प्राकृतिक समाधान
तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में मैंग्रोव ने लगातार अपना महत्व साबित किया है। उदाहरण के लिए, ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घने मैंग्रोव आवरण के कारण चक्रवात दाना का प्रभाव कम हो गया था। एक सरकारी रिपोर्ट बताती है कि अम्फान और यास जैसे चक्रवातों के दौरान घने मैंग्रोव वाले क्षेत्र अधिक सुरक्षित रहे।
भारत वैश्विक मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (एमएसी) का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 15 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव को संरक्षित करना है। हालांकि, एमएसी के तहत एक लोकप्रिय रणनीति है बड़े पैमाने पर रोपण, जो अक्सर निराशाजनक परिणाम देती है। उदाहरण के लिए, 2020 में चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल ने लाखों मैंग्रोव पौधे लगाए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में केवल 15% ही बचे।
बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की चुनौतियाँ
बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वृक्षारोपण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नए लगाए गए मैंग्रोव अक्सर कटाव वाले क्षेत्रों या उच्च ज्वारीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में विफल हो जाते हैं। दुनिया भर में इसी तरह की विफलताओं की सूचना मिली है। केन्या में बड़े पैमाने पर लगाए गए मैंग्रोव पौधों में केवल 30-32% ही जीवित रहते हैं, जबकि श्रीलंका में सुनामी के बाद केवल 3% ही जीवित बचे थे।
श्रीलंका ने 2015 में वैज्ञानिक संरक्षण की ओर रुख किया, और मौजूदा मैंग्रोव के पोषण और प्राकृतिक पुनर्जनन पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरीके से 500 हेक्टेयर से अधिक मैंग्रोव को सफलतापूर्वक बहाल किया गया है और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के रूप में मान्यता प्राप्त की है।
अनियंत्रित शहरीकरण का प्रभाव
शहरीकरण ने मैंग्रोव इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, विशेष रूप से मुंबई में, जहां शहर की सीमा के भीतर 15-20% और महानगरीय क्षेत्र में 40% तक मैंग्रोव नष्ट हो गए हैं। मैंग्रोव विनाश को रोकने के लिए संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे 650 सीसीटीवी कैमरे लगकर मॉनिटरिंग आदि, लेकिन नियमों का पालन कराने और फंडिंग की चुनौतियां बनी हुई हैं।
भारत की लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी पश्चिमी तटरेखा के लिए मैंग्रोव महत्वपूर्ण हैं, जो ढाई करोड़ लोगों का भरण-पोषण करते हैं। पिछले दो दशकों में अरब सागर में चक्रवाती तूफानों में 52% की वृद्धि देखी गई है, जो दर्शाता है कि मैंग्रोव संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।
मैंग्रोव: प्राकृतिक आवास में आबाद
मुंबई से 2,000 किमी दूर – भारत के पूर्वी तट पर – सुंदरबन में कुछ जवाब मिलते हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव वन है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है।
यहां रामगंगा गांव में नदी का किनारा एक प्राचीन ग्रामीण पेंटिंग की तरह लगता है – कंक्रीट के तटबंध के चारों ओर तीन हेक्टेयर तक फैली एक हरी-भरी मैंग्रोव की पट्टी। मैंग्रोव की तीस अलग-अलग प्रजातियाँ यहां खड़ी हैं -जो पथार प्रतिमा ब्लॉक के गाँव में मिलने वाली चार नदियों की बड़ी कटाव शक्तियों के खिलाफ एक आवश्यक सुरक्षा दीवार बनाती हैं।
यह कल्पना करना कठिन है कि ज़मीन का यह टुकड़ा कुछ साल पहले ही बंजर था।
यह उन 31 साइटों में से एक है जिसे पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर कृष्णा रे 2013 से विकसित कर रही हैं। डॉ. रे मैंग्रोव वृक्षारोपण और बहाली के लिए वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाती हैं। मैंग्रोव के बड़े पैमाने पर रोपण के बजाय, वह पहले उनके जीवित रहने और फिर पनपने के लिए सही वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
पहली बात, मैंग्रोव बिना अधिक हस्तक्षेप के अपने प्राकृतिक आवास में प्रचुर मात्रा में आबाद हो सकते हैं। मलेशिया के पश्चिमी तट पर किए गए एक प्रयोग में पाया गया कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को नए वृक्षारोपण के बिना, केवल एक ब्रेकवाटर खड़ा करके और मैंग्रोव विकास के लिए अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान करके पुनर्जीवित किया जा सकता है।
दूसरे, नए वृक्षारोपण की सफलता दर एक समान नहीं होती है क्योंकि सभी पौधे पूर्ण वृक्ष नहीं बन पाते हैं। बहुत कुछ उन क्षेत्रों में ज्वारीय प्रभाव और कटाव पर निर्भर करता है।
तीसरा, यदि एक या कुछ व्यापक रूप से उपलब्ध मैंग्रोव की किस्में लगाई जायें तो , तो परिणाम उतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इससे एक विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बन पायेगा।
डॉ रे कहती हैं, “कुछ मैंग्रोव प्रजातियाँ उच्च लवणता वाली मिट्टी में उगती हैं, जबकि अन्य की उपज मीठे जल क्षेत्रों में अधिक होती है। इसलिए, अधिक दक्षता के लिए, क्षेत्रों को लवणता के अनुसार मैप करना होगा, और फिर उपयुक्त प्रजातियों को रोपना होगा।”
दुरबाकोटी में 5 वर्ष पुरानी साइट पर यह साफ दिखता है। हाथ से लगाई गई घास की कतारें नदी की ओर फैली हुई हैं, जबकि घना मैंग्रोव जंगल तटबंध क बचाये हुए है।
वैज्ञानिक दखल के प्रभाव
डॉ रे कहती हैं, “हम पहले पूरी तरह से बंजर मिट्टी के मैदान पर घास लगाते हैं। ये पोषक तत्वों को बढ़ाकर मिट्टी को समृद्ध करते हैं, जिससे यह जगह पेड़ लगाने के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है। फिर, हम स्थानीय रूप से उपलब्ध मैंग्रोव प्रजातियों का प्रत्यारोपण करते हैं, और कुछ विश्व स्तर पर विलुप्त हो रही प्रजातियों को पहली बार यहां रोपा जाता है। इससे जैव विविधता बढ़ती है, चक्र पुनर्जीवित होता है।”
घास एक महत्वपूर्ण सू्त्रधार है, खासकर जब मडफ्लैट पर मैंग्रोव उगाते हैं, जहां वे पारंपरिक रूप से नहीं होते । इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार, मडफ्लैट्स “क्षरण और जल तरंगों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं”, और “निरंतर नमी के कारण कम ऑक्सीजन सामग्री के परिणामस्वरूप उच्च अंकुरण मृत्यु और अवरुद्ध विकास हो सकता है”।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाधान अत्यधिक स्थानीय होना चाहिए – स्थान की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार बदलाव किया जाना चाहिए, भले ही वह बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो।
मैंग्रोव संरक्षण विशेषज्ञ नरेंद्रन राजेंद्रन – जो तमिलनाडु में रहते हैं – के अनुसार, “संरक्षणवादियों के लिए एक मुख्य नियम होना चाहिए कि वो स्थानीय समुदायों से जानकारी एकत्र करें कि पुरातनकाल से वहां कौन सी मैंग्रोव प्रजातियां मौजूद रही हैं।”
तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में पारंगीपेट्टई में चार स्थलों पर राजेंद्रन की विज्ञान आधारित कोशिशों से 90% नए लगाए गए मैंग्रोव जीवित रहे। लगभग सात साल पहले लगाए गए, ये स्थल इतने घने जंगलों में बदल गए हैं कि अब वह खुद इन स्थलों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और मैंग्रोव अपने आप ही बढ़ते जा रहे हैं।
वह बताते हैं, “मिट्टी की हाइड्रोग्राफी और पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर ही प्रजातियों को रोपा जाना चाहिए। हम मिट्टी की शीर्ष परत को 15-30 सेमी को खोदते हैं, पोषक तत्वों के स्तर का अध्ययन करते हैं, और केकड़े के बिलों का करीबी से निरीक्षण करते हैं – अगर वह अधिक हैं तो इसका मतलब अधिक जैव विविधता है।”
इसका प्रमाण श्रीलंका के सफल मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान में दिया जा सकता है। इसके दिशानिर्देश दस्तावेज़ में बताया गया है कि प्रभावी मैंग्रोव बहाली के लिए किन तत्वों का अध्ययन किया जाना चाहिए। “मैंग्रोव प्रजातियाँ लवणता, पीएच, मिट्टी की नमी के स्तर और एरोबिक मिट्टी की परत की गहराई के अनुसार वितरित होती हैं। इसलिए, प्रभावी बहाली के लिए इन मापदंडों को पहले से मापा जाना चाहिए, ”यह बताता है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि समानांतर रूप से, लवणता का स्तर, ज्वारीय उतार-चढ़ाव, हवा और सूरज की रोशनी की तीव्रता भी मैंग्रोव विकास को प्रभावित करती है, और इसलिए, बहाली के प्रयास।
हीरा है सदा के लिए
पॉलिसी के स्तर पर आम धारणा यह है कि मैंग्रोव ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने और वायुमंडल में कार्बन के स्तर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बड़े विशाल कार्बन सिंक हैं। एक अन्य प्रत्यक्ष लाभ बढ़ते समुद्र और चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाओं के खिलाफ तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा है।
लेकिन अगर मैंग्रोव वन प्राचीन हों तो उसके कहीं अधिक फायदे हैं। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन, जिसमें चार दशकों के डेटा का विश्लेषण किया गया, में पाया गया कि लगाए गए मैंग्रोव अक्षुण्ण, परिपक्व पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले कार्बन स्टॉक का 75% तक संग्रहीत होते हैं।
नदी किनारे के लोगों और तटीय समुदायों की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। मछली पकड़ने और शहद इकट्ठा करने से लेकर लकड़ी की प्रचुर आपूर्ति तक, अप्रत्यक्ष लाभ कई गुना हैं, जो इन हाशिए पर रहने वाले लोगों को बहुत आवश्यक आय स्रोत प्रदान कर सकते हैं।
लेकिन मैंग्रोव का एक मोनोटाइपिक संरक्षण हो तो ज़रूरी नहीं कि ये सभी लाभ मिलेंगे । एक साइट पर जो कि डॉ. रे की टीम द्वारा नहीं देखी जा रही थी, उसमें केवल तीन प्रकार के मैंग्रोव थे जो बढ़ते पानी के खिलाफ बुनियादी सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन वहां कोई अंडरग्रोथ नहीं थी। यहां तलछट को बरकरार रखने या अन्य पौधों को विकसित होने की संभावना नहीं बन पा रही थी, और इस प्रकार कोई जैव विविधता नहीं रही।
एक और महत्वपूर्ण बात यह कि मैंग्रोव हर जगह नहीं लगाए जा सकते। पौधों के पेड़ बनने की सफलता दर अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होती है। यहां तक कि सुंदरबन जैसे एक जंगल में भी स्थितियां काफी भिन्न हो सकती हैं।
रामगंगा के पश्चिम में लगभग 30 किमी दूर, सागर द्वीप पर, नए पेड़ लगाना बिल्कुल व्यर्थ है। वजह साफ है। आईआईएसईआर, कोलकाता के जैविक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. पुण्यस्लोके भादुड़ी कहते हैं, “चूंकि लहरें बहुत तेज़ हैं, इसलिए नए मैंग्रोव जीवित नहीं रह पाएंगे।”
नए पेड़ लगाने के बजाय, वह 25-30 साल पुराने मैंग्रोव पेड़ों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो किसी तरह विनाशकारी चक्रवात अम्फान की तबाही से बचने में कामयाब रहे। उनके प्रयास सागर द्वीप के प्रवेश द्वारों में से एक चेमागुड़ी क्षेत्र में सफल रहे हैं।
डॉ भादुड़ी कहते हैं, “इन मैंग्रोवों की ज़िदा रहने की ताकत अधिक है। इसलिए हम उन्हें पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं. हमने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यहां कटाव और समुद्र स्तर में वृद्धि का स्तर सबसे अधिक है। चक्रवात अम्फान ने इस हिस्से को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन हमारी टीम के हस्तक्षेप से स्थितियों में सुधार हुआ है। अब, चेमागुरी सागर द्वीप में सबसे घने मैंग्रोव हैं, जो लगभग 2-3 वर्ग किमी में फैले हैं। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे केकड़े पकड़ने के लिए यहां आते हैं।”